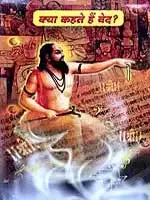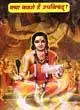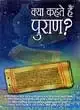|
विवेचनात्मक व उपदेशात्मक संग्रह >> क्या कहते हैं वेद क्या कहते हैं वेदमहेश शर्मा
|
324 पाठक हैं |
||||||
सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है - "ज्ञान"...
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
वेदों में परम सत्य ईश्वर की वाणी संगृहीत की गई है। वेद हमारी प्राचीन
भारतीय संस्कृति और अक्षुण्य भण्डार हैं।
हमारे ऋषि-मुनियों ने युगों तक गहन चिंतन-मनन कर इस ब्रह्माण्ड में उपस्थित कण-कण के गूढ़ रहस्य का सत्यज्ञान वेदों में संगृहीत किया। उन्होंने अपना समस्त जीवन इन गूढ़ रहस्यों को खोजने में लगाकर भारतीय प्रथा, संस्कृति और परम्पराओं की नींव सुदृढ़ की। इन गूढ़ रहस्यों का विश्व के अनेक देशों के विद्वानों ने अध्ययन कर अपने-अपने देशों का विकास किया। चाहे वह चिकित्सा, औषधि शास्त्र का क्षेत्र हो या खगोल शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का हो अथवा साहित्य का। उन्होंने भारतीय ऋषियों की कठिन तपस्या का भरपूर लाभ उठाया और उसे अपनाया भी। बहुत से देशों के विद्वान आज भी इनका अध्ययन कर रहे हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन भारतीय आम लोग वेदों की दुरूहता के कारण इनके संगृहीत गूढ़ रहस्यों का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि उन्हें स्कूल, कॉलेज से ही वैदिक संस्कृति का अनिवार्य रुप से उचित अध्ययन करवाया जाने लगे तो उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएँ और उनकी रुचि भारतीय संस्कृति के सवंर्धन तथा अंगीकरण में संलग्न हो जाए।
संक्षेप में कहें तो वेद ज्ञान के वे भण्डार हैं जिनके उचित अध्ययन के लिए मनुष्य यदि उनमें प्रवेश करे तो वह बनकर निकलेगा और स्वयं का तो उद्धार करेगा ही साथ में औरों का भी उद्धार करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर वेदों के ज्ञान को हमने सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है, यह पुस्तक पाठकों के लिए शिक्षाप्रद, रोचक और उपयोगी सिद्ध होगी। अपनी प्रेरक प्रतिक्रियाओं और सुझावों से अवश्य अवगत् कराएँ।
हमारे ऋषि-मुनियों ने युगों तक गहन चिंतन-मनन कर इस ब्रह्माण्ड में उपस्थित कण-कण के गूढ़ रहस्य का सत्यज्ञान वेदों में संगृहीत किया। उन्होंने अपना समस्त जीवन इन गूढ़ रहस्यों को खोजने में लगाकर भारतीय प्रथा, संस्कृति और परम्पराओं की नींव सुदृढ़ की। इन गूढ़ रहस्यों का विश्व के अनेक देशों के विद्वानों ने अध्ययन कर अपने-अपने देशों का विकास किया। चाहे वह चिकित्सा, औषधि शास्त्र का क्षेत्र हो या खगोल शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का हो अथवा साहित्य का। उन्होंने भारतीय ऋषियों की कठिन तपस्या का भरपूर लाभ उठाया और उसे अपनाया भी। बहुत से देशों के विद्वान आज भी इनका अध्ययन कर रहे हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन भारतीय आम लोग वेदों की दुरूहता के कारण इनके संगृहीत गूढ़ रहस्यों का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि उन्हें स्कूल, कॉलेज से ही वैदिक संस्कृति का अनिवार्य रुप से उचित अध्ययन करवाया जाने लगे तो उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएँ और उनकी रुचि भारतीय संस्कृति के सवंर्धन तथा अंगीकरण में संलग्न हो जाए।
संक्षेप में कहें तो वेद ज्ञान के वे भण्डार हैं जिनके उचित अध्ययन के लिए मनुष्य यदि उनमें प्रवेश करे तो वह बनकर निकलेगा और स्वयं का तो उद्धार करेगा ही साथ में औरों का भी उद्धार करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर वेदों के ज्ञान को हमने सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है, यह पुस्तक पाठकों के लिए शिक्षाप्रद, रोचक और उपयोगी सिद्ध होगी। अपनी प्रेरक प्रतिक्रियाओं और सुझावों से अवश्य अवगत् कराएँ।
महेश शर्मा
लेखक परिचय
महेश शर्मा हिन्दी भाषा के एक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। भारत की अनेक
प्रमुख हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में आपकी तीन हज़ार से अधिक विविध विषयी
रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका लेखन कार्य सन् 1983 से आरंभ हुआ जब आप
हाई स्कूल में अध्ययनरत थे। बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को आपने 1989
में हिन्दी में एम.ए. किया। उसके बाद कुछ वर्षों तक विभिन्न
पत्र-पत्रिकाओं के लिए संवाददाता, सम्पादक और प्रतिनिधि के रूप में कार्य
किया।
आपने विभिन्न विषयों पर अधिकारपूर्वक कलम चलाई और इस समय आपकी लिखी व सम्पादित की चार सौ से अधिक पुस्तकें बाज़ार में हैं।
हिन्दी लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपने अनेक पुरस्कार भी अर्जित किए; जिनमें प्रमुख हैं-नटराज कला संस्थान, झाँसी द्वारा लेखन के क्षेत्र में ‘यूथ अवार्ड’, हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा ‘प्रशंसा पुरस्कार’, अंतर्धारा समाचार व फीचर सेवा, दिल्ली द्वारा ‘लेखक रत्न’ पुरस्कार आदि।
आपने विभिन्न विषयों पर अधिकारपूर्वक कलम चलाई और इस समय आपकी लिखी व सम्पादित की चार सौ से अधिक पुस्तकें बाज़ार में हैं।
हिन्दी लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपने अनेक पुरस्कार भी अर्जित किए; जिनमें प्रमुख हैं-नटराज कला संस्थान, झाँसी द्वारा लेखन के क्षेत्र में ‘यूथ अवार्ड’, हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा ‘प्रशंसा पुरस्कार’, अंतर्धारा समाचार व फीचर सेवा, दिल्ली द्वारा ‘लेखक रत्न’ पुरस्कार आदि।
प्रकाशक
अध्याय 1
परिचय
सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है-‘ज्ञान’। वस्तुतः
ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य-मन के अज्ञानरूपी अंधकार को नष्ट कर देता
है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है, जो पौराणिक ज्ञान-विज्ञान
का अथाह भंडार है। ‘वेद’ शब्द संस्कृत के विद् शब्द
से निर्मित है अर्थात् इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित
है। प्राचीन भारतीय ऋषि जिन्हें मंत्रदृष्टा कहा गया है, उन्होंने मंत्रों
के गूढ़ रहस्यों को जान कर, समझ कर, मनन कर, उनकी अनुभूति कर उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर संसार के समक्ष प्रस्तुत किया वे प्राचीन ग्रंथ
‘वेद’ कहलाए। यहाँ वेद का अर्थ उन्हीं प्राचीन ग्रंथों से है। इस जगत्, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर; इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है।
वेद क्या है ?
वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ हैं, जिनमें ज्योतिष, संगीत, गणित,
विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि लगभग सभी विषयों से
संबंधित ज्ञान का भण्डार भरा पड़ा है। वेद हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़
है। इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय तथा जो इच्छा हो उसके अनुसार उन्हें
प्राप्त करने के उपाय संगृहीत हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में
मेहनत लगती है, उसी प्रकार इन रत्नरूपी वेदों का श्रमपूर्वक अध्ययन करके
ही इनमें संकलित ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। विभिन्न विद्वानों
ने अपने-अपने शब्दों में कहा है कि वेद क्या है ? आइए पढ़ें किसने क्या
कहा है-
(1) मनु के अनुसार, ‘‘सभी धर्म वेद पर आधारित हैं।’’
(2) स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, ‘‘वेद ईश्वरीय ज्ञान है।’’
(3) महर्षि दयानन्द के अनुसार, ‘‘समस्त ज्ञान विद्याओं का निचोड़ वेदों में निहित है।’’
(4) प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के अनुसार,
‘‘वेद-वेद के मंत्र-मंत्र में, मंत्र-मंत्र की पंक्ति-पंक्ति में,
पंक्ति-पंक्ति के शब्द-शब्द में, शब्द-शब्द के अक्षर स्वर में,
दिव्य ज्ञान-आलोक प्रदीपित, सत्यं शिवं सुन्दरं शोभित
कपिल, कणाद और जैमिनि की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन
विशद-विवेचन, प्रत्यालोचन ब्रह्म, जगत्, माया का दर्शन।’’
अर्थात् वेद केवल ढकोसला मात्र नहीं है, इनमें वह पौराणिक ज्ञान समाहित है जिनके अध्ययन से धीरे-धीरे विकास हुआ और आज के आधुनिक युग की कई वस्तुओं का ज्ञान प्राचीन भारतीय ऋषियों ने पहले ही मनन कर प्राप्त कर लिया था। वेद परम शक्तिमान ईश्वर की वाणी है। अर्थात् वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद श्रुति भी कहलाते हैं क्योंकि श्रुति का तात्पर्य है-सुनना। इसका अर्थ है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मनन एवं ध्यान कर अपनी तपस्या के बल पर ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण किया, उसे आत्मसात् किया। जब उनके शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करते तो वे उसी ज्ञान को उन्हें बाँटते।
यह ईश्वररीय ज्ञान मंत्रों के रूप में ऋषियों के साथ सभी को स्मरण होता गया, उन्हें कण्ठस्थ हो गया और धीरे-धीरे उन सभी से एक-दूसरे के पास पहुँचा। क्योंकि प्राचीन काल में आज की तरह स्कूल, कॉलेज नहीं थे। अपितु शिष्य, ऋषियों के आश्रय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे जो गुरु-शिष्य परम्परा कहलाती थी और ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर शिष्यों को समझाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषियों ने जो ईश्वरीय ज्ञान सुना वह वेद है, श्रुति है। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया।
वेद ज्ञान का अनन्त भण्डार है। ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये कोई ऐतिहासिक पुस्तकें नहीं है कि कोई घटना घटी और पुस्तकवद्ध हो गई। अतः ईश्वर की अलौकिक वाणी जो ज्ञानरूप में वेदों में निहित है, उसे समझने के लिए वेद ही वे अलौकिक नेत्र हैं जिनकी सहायता से मनुष्य ईश्वर के अलौकिक ज्ञान को समझ सकता है। वेद ही वे ज्ञान ग्रंथ हैं जिनके समकक्ष विश्व का कोई भी ग्रंथ नहीं है।
अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान है और उनका उद्भव भी ईश्वर द्वारा ही हुआ है।
(1) मनु के अनुसार, ‘‘सभी धर्म वेद पर आधारित हैं।’’
(2) स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, ‘‘वेद ईश्वरीय ज्ञान है।’’
(3) महर्षि दयानन्द के अनुसार, ‘‘समस्त ज्ञान विद्याओं का निचोड़ वेदों में निहित है।’’
(4) प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के अनुसार,
‘‘वेद-वेद के मंत्र-मंत्र में, मंत्र-मंत्र की पंक्ति-पंक्ति में,
पंक्ति-पंक्ति के शब्द-शब्द में, शब्द-शब्द के अक्षर स्वर में,
दिव्य ज्ञान-आलोक प्रदीपित, सत्यं शिवं सुन्दरं शोभित
कपिल, कणाद और जैमिनि की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन
विशद-विवेचन, प्रत्यालोचन ब्रह्म, जगत्, माया का दर्शन।’’
अर्थात् वेद केवल ढकोसला मात्र नहीं है, इनमें वह पौराणिक ज्ञान समाहित है जिनके अध्ययन से धीरे-धीरे विकास हुआ और आज के आधुनिक युग की कई वस्तुओं का ज्ञान प्राचीन भारतीय ऋषियों ने पहले ही मनन कर प्राप्त कर लिया था। वेद परम शक्तिमान ईश्वर की वाणी है। अर्थात् वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद श्रुति भी कहलाते हैं क्योंकि श्रुति का तात्पर्य है-सुनना। इसका अर्थ है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मनन एवं ध्यान कर अपनी तपस्या के बल पर ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण किया, उसे आत्मसात् किया। जब उनके शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करते तो वे उसी ज्ञान को उन्हें बाँटते।
यह ईश्वररीय ज्ञान मंत्रों के रूप में ऋषियों के साथ सभी को स्मरण होता गया, उन्हें कण्ठस्थ हो गया और धीरे-धीरे उन सभी से एक-दूसरे के पास पहुँचा। क्योंकि प्राचीन काल में आज की तरह स्कूल, कॉलेज नहीं थे। अपितु शिष्य, ऋषियों के आश्रय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे जो गुरु-शिष्य परम्परा कहलाती थी और ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर शिष्यों को समझाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषियों ने जो ईश्वरीय ज्ञान सुना वह वेद है, श्रुति है। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया।
वेद ज्ञान का अनन्त भण्डार है। ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये कोई ऐतिहासिक पुस्तकें नहीं है कि कोई घटना घटी और पुस्तकवद्ध हो गई। अतः ईश्वर की अलौकिक वाणी जो ज्ञानरूप में वेदों में निहित है, उसे समझने के लिए वेद ही वे अलौकिक नेत्र हैं जिनकी सहायता से मनुष्य ईश्वर के अलौकिक ज्ञान को समझ सकता है। वेद ही वे ज्ञान ग्रंथ हैं जिनके समकक्ष विश्व का कोई भी ग्रंथ नहीं है।
अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान है और उनका उद्भव भी ईश्वर द्वारा ही हुआ है।
वेदों की उत्पत्ति का पौराणिक आधार
ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना के समय देवों और मनुष्यों के साथ-साथ कुछ असुरों
की भी रचना कर दी। इन असुरों में देवों के विपरीत आसुरी गुणों का समावेश
था, इस कारण ये स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अत्याचारी और अधर्मी हो गए।
ब्रह्माजी ने देवगण के लिए स्वर्ग और मनुष्यों के लिए पृथ्वी की रचना की।
लेकिन जब ब्रह्माजी को असुरों की आसुरी मानसिकता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने
असुरों को पाताल में निवास करने के लिए भेज दिया।
असुर स्वच्छंद आचरण करते थे। शीघ्र ही उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान् शिव को प्रसन्न कर वरदान में अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर लीं और पृथ्वी पर आकर ऋषि-मुनियों पर अत्याचार करने लगे। धीरे-धीरे ये अत्याचार बढ़ते गए। इससे असुरों की आसुरी शक्तियों में भी वृद्धि होती गई। देवों की शक्ति का आधार भक्ति, सात्त्विकता और धर्म था, लेकिन स्वर्ग के भोग-विलास में डूबकर वे इसे भूल गए, इस कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई।
देवों को शक्तिहीन देखकर दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों वर्षों तक देवों और असुरों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण अंत में देवों की पराजय हुई और वे प्राण बचाते हुए स्वर्ग से भाग खड़े हुए। इस प्रकार शक्तिसंपन्न असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया।
इधर, इन्द्रादि देवगण अपनी रक्षा करने के लिए भगवान् शिव के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान् शिव ने जब देवों से वहाँ आने का कारण पूछा तो देवराज इंद्र बोले-‘‘भगवान् ! आपके द्वारा वरदान प्रदान करने से असुर शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और हमें मारने का संकल्प किया है। आप हमारी रक्षा करें प्रभु।’’
देवों की करुण पुकार सुनकर शिव जी बोले-‘‘देवगण ! भोग-विलास और ऐश्वर्य में डूबे रहने के कारण तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, जबकि असुर अपनी तपस्या के बल से परमबलशाली हो गए हैं। तुम्हारी रक्षा अब केवल माता गायत्री ही कर सकती हैं। अतः आप सब माता गायत्री की शरण में जाएँ।’’
तब भगवान् शिव सहित सभी देवगण भगवती गायत्री के सम्मुख उपस्थित हुए और उनकी पूजा-अर्चना की। भगवती गायत्री के प्रसन्न होने पर भगवान् शिव बोले-‘‘हे माते ! तीनों लोकों में असुरों के अत्याचारों से हाहाकार मच गया है। आसुरी शक्तियाँ दैवीय शक्तियों से अधिक बलशाली हो गई हैं। देवों को शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी पर भक्ति, सात्त्विकता, धर्म और सदाचार की स्थापना की जाए, जिससे दैवीय शक्तियों को बल प्राप्त हो और वे शक्तिशाली होकर आसुरी शक्ति को पराजित कर सकें।’’
देवों की करुण विनती सुनकर भगवती गायत्री बोलीं-‘‘हे देवगण ! आप निश्चिंत रहें। मैं वैदिक और धार्मिक शक्तियों द्वारा चार वैदिक पुत्रों को जन्म दूँगी, जो भक्ति, धर्म, न्याय और सदाचार की स्थापना करते हुए देवों को शक्ति प्रदान, कर शक्तिसम्पन्न बनाएँगे।’’
इतना कहने के बाद देवी गायत्री ने नेत्र बंद कर अपनी वैदिक और धार्मिक शक्तियों को मस्तिष्क में केन्द्रित किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले। नेत्रों के खुलते ही उनमें से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज में से निकलने वाली तेज किरणें सभी दिशाओं को आलोकित करने लगीं। वह प्रकाश पुंज इतना अधिक तेजयुक्त था कि ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण प्रकाश भी उसके समक्ष प्रभाहीन हो गया।
तत्पश्चात् इस प्रकाश-पुंज में से चार दिव्य बालकों-ऋग्, यजु, अथर्व और साम का जन्म हुआ। भगवती गायत्री की वैदिक और धार्मिक शक्तियों के कारण ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए ये चारों बालक वेद और भगवती गायत्री वेदों की माता कहलाईं।
दिव्य बालकों के जन्म लेते ही भगवती गायत्री उनसे बोलीं-‘‘हे पुत्रों ! तुम्हारा जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। आज से तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन पृथ्वी पर धर्म और भक्ति के प्रचार में व्यतीत होगा। जब तक संसार में तुम चारों का अस्तित्व रहेगा, तब तक पृथ्वी पर तामसिक शक्तियाँ श्रीहीन रहेंगी। असत्य पर सदा सत्य की विजय होगी।’’
भगवती गायत्री से अपने जन्म का उद्देश्य जानकर चारों दिव्य बालक पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही दिनों के बाद वेदों के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर सात्त्विक शक्तियों का प्रसार होने लगा। ऋषि-मुनि यज्ञ और अनुष्ठान करने लगे, जिनसे शक्ति प्राप्त कर देवगण शक्तिशाली होते गए। शीघ्र ही देवों ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। इस बार असुरों की तामसिक शक्तियाँ देवों की सात्त्विक शक्तियों के समक्ष टिक न सकीं और असुरों को पराजित होकर पाताल में भागना पड़ा। स्वर्ग पर पुनः देवों का अधिकार हो गया।
असुर स्वच्छंद आचरण करते थे। शीघ्र ही उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान् शिव को प्रसन्न कर वरदान में अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर लीं और पृथ्वी पर आकर ऋषि-मुनियों पर अत्याचार करने लगे। धीरे-धीरे ये अत्याचार बढ़ते गए। इससे असुरों की आसुरी शक्तियों में भी वृद्धि होती गई। देवों की शक्ति का आधार भक्ति, सात्त्विकता और धर्म था, लेकिन स्वर्ग के भोग-विलास में डूबकर वे इसे भूल गए, इस कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई।
देवों को शक्तिहीन देखकर दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों वर्षों तक देवों और असुरों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण अंत में देवों की पराजय हुई और वे प्राण बचाते हुए स्वर्ग से भाग खड़े हुए। इस प्रकार शक्तिसंपन्न असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया।
इधर, इन्द्रादि देवगण अपनी रक्षा करने के लिए भगवान् शिव के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान् शिव ने जब देवों से वहाँ आने का कारण पूछा तो देवराज इंद्र बोले-‘‘भगवान् ! आपके द्वारा वरदान प्रदान करने से असुर शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और हमें मारने का संकल्प किया है। आप हमारी रक्षा करें प्रभु।’’
देवों की करुण पुकार सुनकर शिव जी बोले-‘‘देवगण ! भोग-विलास और ऐश्वर्य में डूबे रहने के कारण तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, जबकि असुर अपनी तपस्या के बल से परमबलशाली हो गए हैं। तुम्हारी रक्षा अब केवल माता गायत्री ही कर सकती हैं। अतः आप सब माता गायत्री की शरण में जाएँ।’’
तब भगवान् शिव सहित सभी देवगण भगवती गायत्री के सम्मुख उपस्थित हुए और उनकी पूजा-अर्चना की। भगवती गायत्री के प्रसन्न होने पर भगवान् शिव बोले-‘‘हे माते ! तीनों लोकों में असुरों के अत्याचारों से हाहाकार मच गया है। आसुरी शक्तियाँ दैवीय शक्तियों से अधिक बलशाली हो गई हैं। देवों को शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी पर भक्ति, सात्त्विकता, धर्म और सदाचार की स्थापना की जाए, जिससे दैवीय शक्तियों को बल प्राप्त हो और वे शक्तिशाली होकर आसुरी शक्ति को पराजित कर सकें।’’
देवों की करुण विनती सुनकर भगवती गायत्री बोलीं-‘‘हे देवगण ! आप निश्चिंत रहें। मैं वैदिक और धार्मिक शक्तियों द्वारा चार वैदिक पुत्रों को जन्म दूँगी, जो भक्ति, धर्म, न्याय और सदाचार की स्थापना करते हुए देवों को शक्ति प्रदान, कर शक्तिसम्पन्न बनाएँगे।’’
इतना कहने के बाद देवी गायत्री ने नेत्र बंद कर अपनी वैदिक और धार्मिक शक्तियों को मस्तिष्क में केन्द्रित किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले। नेत्रों के खुलते ही उनमें से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज में से निकलने वाली तेज किरणें सभी दिशाओं को आलोकित करने लगीं। वह प्रकाश पुंज इतना अधिक तेजयुक्त था कि ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण प्रकाश भी उसके समक्ष प्रभाहीन हो गया।
तत्पश्चात् इस प्रकाश-पुंज में से चार दिव्य बालकों-ऋग्, यजु, अथर्व और साम का जन्म हुआ। भगवती गायत्री की वैदिक और धार्मिक शक्तियों के कारण ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए ये चारों बालक वेद और भगवती गायत्री वेदों की माता कहलाईं।
दिव्य बालकों के जन्म लेते ही भगवती गायत्री उनसे बोलीं-‘‘हे पुत्रों ! तुम्हारा जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। आज से तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन पृथ्वी पर धर्म और भक्ति के प्रचार में व्यतीत होगा। जब तक संसार में तुम चारों का अस्तित्व रहेगा, तब तक पृथ्वी पर तामसिक शक्तियाँ श्रीहीन रहेंगी। असत्य पर सदा सत्य की विजय होगी।’’
भगवती गायत्री से अपने जन्म का उद्देश्य जानकर चारों दिव्य बालक पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही दिनों के बाद वेदों के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर सात्त्विक शक्तियों का प्रसार होने लगा। ऋषि-मुनि यज्ञ और अनुष्ठान करने लगे, जिनसे शक्ति प्राप्त कर देवगण शक्तिशाली होते गए। शीघ्र ही देवों ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। इस बार असुरों की तामसिक शक्तियाँ देवों की सात्त्विक शक्तियों के समक्ष टिक न सकीं और असुरों को पराजित होकर पाताल में भागना पड़ा। स्वर्ग पर पुनः देवों का अधिकार हो गया।
वेद मंत्रों का संकलन और वेदों की संख्या
ऐसी मान्यता है कि वेद प्रारम्भ में एक ही था और उसे पढ़ने के लिए
सुविधानुसार चार भागों में विभक्त कर दिया गया। ऐसा श्रीमद्भागवत में
उल्लेखित एक श्लोक द्वारा भी स्पष्ट होता है। इन वेदों में हज़ारों मंत्र
और ऋचाएँ हैं जो एक ही समय में संभवतः नहीं रची गई होंगी और न ही एक ऋषि
द्वारा। इनकी रचना समय-समय पर ऋषियों द्वारा होती रही और वे एकत्रित होते
गए।
शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया।
शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया।
‘‘अग्निवायुरविभ्यस्तुत्नयं ब्रह्म सनातनम।
दुदोह यत्रसिद्वद्धथमृग्यजुः सामलक्षणम्।।
दुदोह यत्रसिद्वद्धथमृग्यजुः सामलक्षणम्।।
मनुस्मृति के इस श्लोक के अनुसार-‘‘सनातन ब्रह्म ने
यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु एवं सूर्य से ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं
सामवेद को व्यक्त किया।’’
अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार-‘‘इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ।’’ अर्थात् मनुस्मृति में प्रथम तीन वेदों को अग्नि, वायु एवं सूर्य से जोड़ा गया है। इन तीनों नामों के ऋषियों से इनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है। इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक माना गया है।
वायु प्रायः चलायमान है। उसका काम चलना (बहना) है। इसका तात्पर्य है कि कर्म अथवा कार्य करते रहना। इसलिए यह कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेजयुक्त है जिसे सभी प्रणाम करते हैं। नतमस्तक होकर उसे पूजते हैं। इसलिए कहा गया है कि वह पूजनीय अर्थात् उपासना के योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्माजी के चार मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई।
प्राचीन काल में महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यासजी थे। वे बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने वेदों के मंत्रों को एकत्रित कर उन्हें चार अलग-अलग वेदों की उनकी विशेषतानुसार संगृहीत किया। उन्होंने इन मंत्रों को संगृहीत कर निम्न चारों वेदों की रचना की और वे इसी कारण वेद व्यास अर्थात् वेदों को विस्तार देने वाले, बाँटने वाले कहलाए।
अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार-‘‘इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ।’’ अर्थात् मनुस्मृति में प्रथम तीन वेदों को अग्नि, वायु एवं सूर्य से जोड़ा गया है। इन तीनों नामों के ऋषियों से इनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है। इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक माना गया है।
वायु प्रायः चलायमान है। उसका काम चलना (बहना) है। इसका तात्पर्य है कि कर्म अथवा कार्य करते रहना। इसलिए यह कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेजयुक्त है जिसे सभी प्रणाम करते हैं। नतमस्तक होकर उसे पूजते हैं। इसलिए कहा गया है कि वह पूजनीय अर्थात् उपासना के योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्माजी के चार मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई।
प्राचीन काल में महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यासजी थे। वे बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने वेदों के मंत्रों को एकत्रित कर उन्हें चार अलग-अलग वेदों की उनकी विशेषतानुसार संगृहीत किया। उन्होंने इन मंत्रों को संगृहीत कर निम्न चारों वेदों की रचना की और वे इसी कारण वेद व्यास अर्थात् वेदों को विस्तार देने वाले, बाँटने वाले कहलाए।
वेदों की संख्या
1-ऋग्वेद 2-यजुर्वेद 3-सामवेद 4-अथर्ववेद
जहाँ तक वेदों की प्रचीनता का प्रश्न है तो वेद 1,96,08,52,976 वर्ष पहले उद्भव हुए। क्योंकि सृष्टि की रचना इतने ही वर्ष पूर्व हुई और ईश्वर ने वेदों के रूप में ऋषियों को यह ज्ञान तभी दिया।
जहाँ तक वेदों की प्रचीनता का प्रश्न है तो वेद 1,96,08,52,976 वर्ष पहले उद्भव हुए। क्योंकि सृष्टि की रचना इतने ही वर्ष पूर्व हुई और ईश्वर ने वेदों के रूप में ऋषियों को यह ज्ञान तभी दिया।
क्या कहते हैं वेद ?
‘‘सर्वेषा तु सा नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथ्क्संस्थाश्च निर्ममे।।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथ्क्संस्थाश्च निर्ममे।।
अर्थात् जब सृष्टि की रचना हुई तो उसके साथ ही वेद के शब्दों द्वारा सभी
नाम अलग-अलग नियत किए गए और उनकी संस्थाएँ भी अलग-अलग नियत की गईं।
अर्थ यह हुआ कि जब सृष्टि की रचना हुई तब वेदों में सभी के लिए नाम, उनके कर्म, उनकी संस्थाओं को अलग-अलग बनाया गया जिससे सभी अपनी-अपनी संस्था, नाम आदि के अनुसार कर्म करें।
वेद के अंदर वह ज्ञान, वह शक्ति है जो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है। यदि सभी को इनका अच्छा ज्ञान हो और मनुष्य उनका अनुसरण करें तो इसी धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। वेद मनुष्य के कल्याण के लिए सभी प्रकार के ज्ञान के भण्डार हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अछूती रही हो और यदि सभी इनका उचित ज्ञान लें तो वे दुःख-अशांति से छुटकारा पा सकते हैं। अर्थात् वेद प्राणी के कल्याण को सर्वोपरि मानकर उसके कल्याण की ही शिक्षा देते हैं।
मनुष्य से संबंधित कोई भी कर्म हो, जैसे-विवाह, मृत्यु, जन्म यज्ञ आदि; वे सभी कार्य मंत्रोच्चाकरण के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। इन मंत्रों की शक्ति से मनुष्य अपने जीवन को तो सुधार ही सकता है साथ ही वह दूसरों का उद्धार भी कर सकता है। ये वेद मंत्र ही हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये मनुष्य के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उपयोगी होते हैं। मनुस्मृति में वेदों को धर्म का मूल अर्थात् जड़ में कहा गया है।
वेद भारतीयों के रग-रग में बसे हैं। इसी कारण से भारत प्राचीन काल से ही समस्त प्राणी जगत् का गुरु रहा है। वेदों में मंत्रों द्वारा देवों की उपासना प्राचीन काल से होती आ रही है। वेदों से ही हिन्दू धर्म की व्यापकता, उदारता, परोपकार, मानव कल्याण तथा साथ ही सभी प्राणियों के कल्याण की भावना पता चलती है। हिन्दू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत एवं पुराणों में धर्म के संबंध में जो भी उल्लेख मिलता है वह वेदों में ही निहित है।
वेदों में केवल धर्म का ही उल्लेख नहीं है; इनमें राजनीति, आचार, आचार-विचार, विज्ञान ज्योतिष, औषधि, दर्शन का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। वेदों में चारों वर्णों, उनके कार्यों, कर्तव्यों और आचरणों का भी उल्लेख है। साथ ही सामजिक आचार-विचार, शिष्टाचार, राष्ट्र रक्षा के उपाय, उस पर शासन करने के सिद्धांत उल्लेखित हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति के लिए सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख है। व्यवसाय, आर्थिक नीतियों का वर्णन है। भूगोल से संबधित ज्ञान भी इसमें विस्तृत प्रतिपादित है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है।
वेदों में वह असीम ज्ञान है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रमाणित है अर्थात् उस समय वेद काल में लगभग सभी आधुनिक आविष्कारों का जन्म हो चुका था जो आज भी वेदों में पढा जा सकता है। वैज्ञानिक भी उन्हें स्वीकारते हैं।
‘‘एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’’
अर्थात् सत्य एक है लेकिन वह अनेक रूपों में विद्यमान है। वैदिक काल में ऋषियों ने ध्यान करने के लिए कहा क्योंकि ध्यान करने से ही मनुष्य का मन एकाग्रचित हो सकता है। तभी वह ईश्वर से संपर्क कर सकता है। ध्यान करने से मनुष्य को इधर-उधर का ध्यान नहीं रहता है और वह केवल एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का ध्यान करता हुआ परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उनके दर्शन करता है। तत्पश्चात् यज्ञ-कर्म आदि पर जोर दिया गया।
प्राचीन काल में वेदों के मंत्रों द्वारा ऋषियों ने जन कल्याण को सबसे ऊपर रखा और तब से वही परम्परा आज तक चली आ रही है। वेदो में ज्ञान तो है ही, साथ इसमें समस्त प्राणी जगत् के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। यही कारण है कि भारत के गौरव ये ग्रंथ भारतीयों को आज तक सर्वोपरि रखे हैं। क्योंकि विश्व का कोई ऐसा ग्रंथ या साहित्य नहीं है जो इतना प्राचीन और इतने गहन अध्ययन के उपरान्त प्रचलन में आया हो। विश्व के सभी विद्वानों ने इन्हीं का अध्ययन कर अपने देशों का निरंतर विकास किया। लेकिन संभवतः इस कारण से इन वेदों को तुच्छ समझा होगा कि यदि हम इतने विकास को इनसे जोड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व ही नगण्य हो जाएगा।
इस प्रकार वेद सम्पूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। सत्य के भंडार हैं। जिन्हें यदि कोई मनन कर अध्ययन करता है तो वह सम्पूर्ण सत्य को प्राप्त करता है। ये वेद इतने प्राचीन हैं लेकिन आज के युग में भी नवीनतम ज्ञान के भण्डार हैं। आज आधुनिकता में मनुष्य को इनका सही ज्ञान नहीं है और वे इन वेदों को मात्र ढकोसला मानते हैं, जबकि सत्यता यह है कि वे लोग अज्ञानी हैं। जो इनका अध्ययन करता है वही इस ईश्वरीय ज्ञान का भागी होता है।
अर्थ यह हुआ कि जब सृष्टि की रचना हुई तब वेदों में सभी के लिए नाम, उनके कर्म, उनकी संस्थाओं को अलग-अलग बनाया गया जिससे सभी अपनी-अपनी संस्था, नाम आदि के अनुसार कर्म करें।
वेद के अंदर वह ज्ञान, वह शक्ति है जो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है। यदि सभी को इनका अच्छा ज्ञान हो और मनुष्य उनका अनुसरण करें तो इसी धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। वेद मनुष्य के कल्याण के लिए सभी प्रकार के ज्ञान के भण्डार हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अछूती रही हो और यदि सभी इनका उचित ज्ञान लें तो वे दुःख-अशांति से छुटकारा पा सकते हैं। अर्थात् वेद प्राणी के कल्याण को सर्वोपरि मानकर उसके कल्याण की ही शिक्षा देते हैं।
मनुष्य से संबंधित कोई भी कर्म हो, जैसे-विवाह, मृत्यु, जन्म यज्ञ आदि; वे सभी कार्य मंत्रोच्चाकरण के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। इन मंत्रों की शक्ति से मनुष्य अपने जीवन को तो सुधार ही सकता है साथ ही वह दूसरों का उद्धार भी कर सकता है। ये वेद मंत्र ही हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये मनुष्य के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उपयोगी होते हैं। मनुस्मृति में वेदों को धर्म का मूल अर्थात् जड़ में कहा गया है।
वेद भारतीयों के रग-रग में बसे हैं। इसी कारण से भारत प्राचीन काल से ही समस्त प्राणी जगत् का गुरु रहा है। वेदों में मंत्रों द्वारा देवों की उपासना प्राचीन काल से होती आ रही है। वेदों से ही हिन्दू धर्म की व्यापकता, उदारता, परोपकार, मानव कल्याण तथा साथ ही सभी प्राणियों के कल्याण की भावना पता चलती है। हिन्दू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत एवं पुराणों में धर्म के संबंध में जो भी उल्लेख मिलता है वह वेदों में ही निहित है।
वेदों में केवल धर्म का ही उल्लेख नहीं है; इनमें राजनीति, आचार, आचार-विचार, विज्ञान ज्योतिष, औषधि, दर्शन का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। वेदों में चारों वर्णों, उनके कार्यों, कर्तव्यों और आचरणों का भी उल्लेख है। साथ ही सामजिक आचार-विचार, शिष्टाचार, राष्ट्र रक्षा के उपाय, उस पर शासन करने के सिद्धांत उल्लेखित हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति के लिए सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख है। व्यवसाय, आर्थिक नीतियों का वर्णन है। भूगोल से संबधित ज्ञान भी इसमें विस्तृत प्रतिपादित है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है।
वेदों में वह असीम ज्ञान है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रमाणित है अर्थात् उस समय वेद काल में लगभग सभी आधुनिक आविष्कारों का जन्म हो चुका था जो आज भी वेदों में पढा जा सकता है। वैज्ञानिक भी उन्हें स्वीकारते हैं।
‘‘एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’’
अर्थात् सत्य एक है लेकिन वह अनेक रूपों में विद्यमान है। वैदिक काल में ऋषियों ने ध्यान करने के लिए कहा क्योंकि ध्यान करने से ही मनुष्य का मन एकाग्रचित हो सकता है। तभी वह ईश्वर से संपर्क कर सकता है। ध्यान करने से मनुष्य को इधर-उधर का ध्यान नहीं रहता है और वह केवल एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का ध्यान करता हुआ परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उनके दर्शन करता है। तत्पश्चात् यज्ञ-कर्म आदि पर जोर दिया गया।
प्राचीन काल में वेदों के मंत्रों द्वारा ऋषियों ने जन कल्याण को सबसे ऊपर रखा और तब से वही परम्परा आज तक चली आ रही है। वेदो में ज्ञान तो है ही, साथ इसमें समस्त प्राणी जगत् के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। यही कारण है कि भारत के गौरव ये ग्रंथ भारतीयों को आज तक सर्वोपरि रखे हैं। क्योंकि विश्व का कोई ऐसा ग्रंथ या साहित्य नहीं है जो इतना प्राचीन और इतने गहन अध्ययन के उपरान्त प्रचलन में आया हो। विश्व के सभी विद्वानों ने इन्हीं का अध्ययन कर अपने देशों का निरंतर विकास किया। लेकिन संभवतः इस कारण से इन वेदों को तुच्छ समझा होगा कि यदि हम इतने विकास को इनसे जोड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व ही नगण्य हो जाएगा।
इस प्रकार वेद सम्पूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। सत्य के भंडार हैं। जिन्हें यदि कोई मनन कर अध्ययन करता है तो वह सम्पूर्ण सत्य को प्राप्त करता है। ये वेद इतने प्राचीन हैं लेकिन आज के युग में भी नवीनतम ज्ञान के भण्डार हैं। आज आधुनिकता में मनुष्य को इनका सही ज्ञान नहीं है और वे इन वेदों को मात्र ढकोसला मानते हैं, जबकि सत्यता यह है कि वे लोग अज्ञानी हैं। जो इनका अध्ययन करता है वही इस ईश्वरीय ज्ञान का भागी होता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book